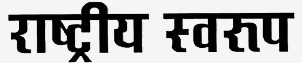जन्माष्टमी 2021: कृष्ण और राधा द्वारा शुरू की गई सांझी कला के स्वरूप में हुए कई परिवर्तन



हमारी अधिकांश लोक कलाओं के केंद्र में कृष्ण और राधा होते हैं। कलाओं के साथ राम और शिव भी जुड़ते हैं, परंतु इतनी गहराई के साथ नहीं जितने कि कृष्ण। इसके पीछे एक ही कारण है कि कृष्ण का जीवन जितना लोक के साथ जुड़ा और लोक उनके साथ जुड़ा, उतना अन्य के साथ नहीं। राम और शिव हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं। उनके पीछे-पीछे चलने का मन होता है, लेकिन कृष्ण के पीछे नहीं, अपितु उनके साथ साथ चलने का मन होता है। उनके साथ गायों के पीछे धूल में नहाने, गेंद खेलने, मटकी फोड़ने तक हम कृष्ण के साथ बराबर के भागीदार बने रहते हैं। लोक जीवन से जुड़े ऐसे कृष्ण लोक कलाओं में यदि अपना प्रभुत्व रखते हैं तो आश्चर्य कैसा?
ऐसी ही एक लोक कला है सांझी कला। मध्य प्रदेश की बार-बार यात्रा करते हुए मालवा क्षेत्र से भी गुजरना हुआ। ट्रेन की यात्रा के बीच खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते दृश्यों को देखना और इसी मनोरंजन के मध्य कच्चे घरों की लिपी-पुती दीवारों पर गोबर की सुंदर कलाकारी मन को कुछ सोचने के लिए विवश करती रही। चित्रकला की अपनी एक प्रोफेसर मित्र से बात की तो सांझी कला के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिली। सांझी कला से जुड़ी एक लोक कथा है। एक दिन राधा कृष्ण से सुबह से शाम तक रूठी रहीं। सांझ की बेला में कृष्ण ने उन्हें मनाने के लिए गोबर और फूलों की पंखुड़ियों से भित्ति पर कुछ आकृतियों का निर्माण किया। इन आकृतियों में सूर्य, चंद्रमा, तिलक, तीर, कमान, सांप, बिच्छू, औरत आदि का भी चित्र बनाया। चित्र को देखकर राधा हंस पड़ीं और तभी से ब्रज तथा उसके आसपास के क्षेत्र में सांझी का अंकन करने की परंपरा प्रारंभ हुई। सांझ के समय खेलने की परंपरा के कारण भी इसका नाम सांझी पड़ा। कृष्ण और राधा द्वारा शुरू की गई इस सांझी कला के स्वरूप में धीरे-धीरे कई परिवर्तन हुए। गोबर से बनाए चित्रों को कौड़ियों, फूलों, चमकीली पन्नियों, रुई आदि से सजाने की परंपरा भी मनुष्य के भीतर की सौंदर्य चेतना का ही प्रतीक है।
भारत में कृष्ण से जुड़ने के कारण ही गाय आयु, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक बनता है। उसमें देवत्व की भावना कृषि और शिल्प प्रधान संपूर्ण भारत राष्ट्र की भावना है। गोवर्धन धारण करने के लिए कृष्ण के गोपाल बनने और ग्वाल बालों के साथ ही गोवंश की रक्षा के संकल्प की भावना है। गायों से अधिक सामीप्य भला कृष्ण का और किसे मिला? राधा और गोपियों का आधा समय मान-मनुहार में बीतता था तो आधा समय कृष्ण के वियोग में। वे गायें ही थीं जो अपनी खुरों से धूल उड़ा-उड़ा कर कृष्ण को रजमय बना देती थीं तो कृष्ण भी अपनी लकुटी से घेर कर उन्हें एक जगह इकट्ठा करते थे। कान्हा को अपने पीछे दौड़ाने का सुख गायों के अलावा भला और कौन पा सका? उन्हीं गायों के गोरस से लेकर गोमय तक पर यदि कृष्ण रीझते रहे और राधा को रिझाते रहे तो आश्चर्य कैसा?
नदियों के संरक्षण का संदेश : भारत की कृषक संस्कृति के साथ पर्यावरण सुरक्षा की प्राचीनतम वैज्ञानिकता के साथ भी कृष्ण जुड़ते हैं। काशी में रामलीला के साथ कृष्ण की बाल लीला नाग नथैया का उत्सव भी गंगा की बीच धारा में मनाए जाने की परंपरा है। पहले सोचती थी कि काशी उत्सव प्रिया नगरी है, शायद इसलिए। परंतु मां गंगा के संदर्भ में जब विचार करना शुरू किया तो प्रतीकार्थ खुलते गए। कृष्ण बना कोई बालक गंगा में कूदता है और कुछ क्षणों में ही एक कृत्रिम सहस्त्रफण वाले कालिया नाग के सिर पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए जल के ऊपर प्रकट होता है। हजारों की संख्या में घाटों पर उपस्थित लीला प्रेमी इस दृश्य को अपनी आंखों में बसाते हैं और हर हर महादेव के जयकारे से गंगा का घाट गूंज उठता है। आस्था और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष गंगा में होती आ रही है यह लीला। कृष्ण का नदी में कूदना और कालिया नाग को नाथ कर उसके सहस्त्रफण पर नाचना एक प्रतीकात्मक बिंब है जिसे आधुनिक युग में भी सभी को समझना पड़ेगा।
दरअसल नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए महापुरुषों द्वारा आगे आने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। कृष्ण उसके प्रतिनिधि हैं। प्रतिवर्ष उस परंपरा को उत्सव रूप में दोहरा कर हम अपने दायित्व से विरत न होने का भाव हृदय में भरते हैं। कृष्ण यमुना से जुड़ते हैं। यमुना के बहाने सभी नदियों को प्रदूषण मुक्ति के उद्देश्य से जुड़ते हैं। हमें सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए उसी प्रकार के नाग नथैया की आवश्यकता है। नाग नथैया यानी नदियों में गिरने वाले हजारों नाग के समान जहरीले जल वाले नाले। यदि नदियों में इन नालों का गिरना रोक दिया जाए तो बहुत हद तक नदियां प्रदूषण से मुक्त हो सकेंगीं। शायद कृष्ण के बहाने हम किसी भी प्रकार के सामाजिक विष के हरण करने की एक सूक्ष्म चेतना से भर जाते हैं- चाहे वह किसी पूतना जैसे विषैले षड्यंत्र से मासूम बच्चों को बचा लेने का उपक्रम हो या फिर यमुना जैसी नदियों में रहने वाले विषैले प्रदूषण कारक। क्या हम समझने को तैयार हैं?